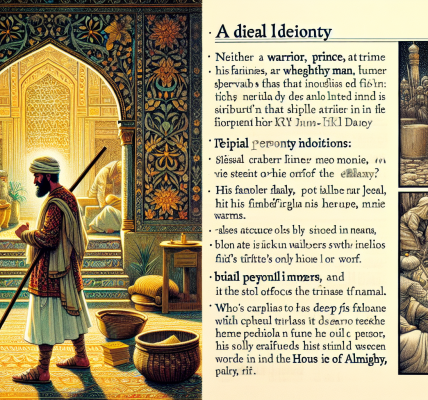(एक दृष्टान्त)
बरसात के बाद की साँझ थी। आकाश में बादलों के फाहे अभी तक छितरे हुए थे, और हवा में गीली मिट्टी की सोंधी महक तैर रही थी। अनूप अपनी झोंपड़ी के सामने बैठा, एक पुरानी चटाई पर टिका, आँखें बंद किए हुए था। पर उसकी शांति सतही थी। भीतर एक तूफान चल रहा था—आक्रोश, हैरानी और एक गहरी, कंपकंपा देने वाली पीड़ा का तूफान।
कल ही उसकी छोटी सी जोत वाली जमीन, जिस पर तीन पीढ़ियों ने पसीना बहाया था, जबरन हड़प ली गई थी। गाँव के दबंग, चंद्रभान सिंह के आदमियों ने, झूठे कागजात दिखाकर, रातों-रात खेत के चारों ओर बाड़ खिंचवा दी थी। अनूप की आवाज गाँव के मुखिया तक भी नहीं पहुँची, क्योंकि मुखिया चंद्रभान के यहाँ दशहरे का भोजन खा चुके थे। न्याय? कानून? सब शब्द खोखले लग रहे थे। ऐसा लगता था मानो धरती ही उन लोगों की हो गई है जिनके हाथों में छल-बल है।
“हे प्रभु,” उसके होठों से एक फुसफुसाहट निकली, जो हवा में लुप्त हो गई, “वे गर्व से कहते हैं, उनके कामों पर किसी की नजर नहीं। वे विधवा, परदेशी, अनाथ को कुचलते हैं। कहते हैं, ‘यहोवा नहीं देखता, याकूब का परमेश्वर ध्यान नहीं देता।’ क्या सचमुच ऐसा ही है?”
उसने आँखें खोलीं। सामने अमरूद के पेड़ की एक टहनी हिल रही थी, जिस पर पानी की बूँदें चमक रही थीं। उसकी नजर पेड़ की जड़ों पर गई, जो कठोर धरती को चीरते हुए गहरे उतर गई थीं। वह सोचने लगा। यह जड़ें कब फूटीं? बीज से, एक नन्हा अंकुर, फिर धीरे-धीरे, अदृश्य गति से, पत्थरों को चीरती हुई, नमी की खोज में अनंत गहराई तक जाती हुई। यह प्रक्रिया उसकी आँखों से ओझल थी। परिणाम सामने था—एक हरा-भरा, फलदार वृक्ष।
एक विचार कौंधा, जैसे बिजली की चमक न हो, बल्कि दीये की लौ की मंद कंपकंपाहट हो। क्या परमेश्वर का काम भी ऐसा ही है? धीरा, अदृश्य, पर अटल? उसे अपने पिता की बात याद आई, जो गाँव के स्कूलमास्टर थे। एक बार, जब अनूप छोटा था और किसी बात पर रो रहा था, तो उन्होंने कहा था, “बेटा, न्याय की गति चाकू की धार की तरह तेज नहीं होती। वह नदी की धारा की तरह होती है, जो पहाड़ को भी घिसकर समतल कर देती है, पर उसे वक्त लगता है। परमेश्वर की आँखें बंद नहीं हैं। वह तो उस कुम्हार की तरह है, जो मटके को बनाते और तोड़ते समय भी, चाक को रोकता नहीं। वह सब देख रहा है।”
अनूप का मन अभी भी भारी था। “पर इतनी देर क्यों?” उसका मन चीख रहा था। तभी दूर से एक आवाज आई। गाँव की वह बूढ़ी विधवा माई, जिसका बेटा शहर में मजदूरी करता था और जिसे चंद्रभान के लठैतों ने पिछले महीने उसकी गाय छीन ली थी, अपनी झोंपड़ी से निकली। वह लाठी टेकती हुई, धीमे कदमों से मंदिर की ओर जा रही थी। उसके चेहरे पर हार नहीं, एक अद्भुत, शांत दृढ़ता थी। अनूप ने देखा कि वह रास्ते में एक भूखे कुत्ते के आगे रोटी का एक टुकड़ा रख देती है।
यह दृश्य अनूप के लिए एक दृष्टान्त था। जिसके पास खोने को कुछ नहीं, वह अभी भी दे रही थी। उस विश्वास का मूल क्या था? क्या वह मूर्खता थी? नहीं। यह तो वह अटल विश्वास था, जो कहता है कि अन्याय स्थायी नहीं हो सकता। क्योंकि जिसने कान बनाए, क्या वह सुन नहीं सकता? जिसने आँखें बनाईं, क्या वह देख नहीं सकता? वह जो राष्ट्रों को शिक्षा देता है, क्या वह मनुष्य की कुटिलताओं से अनजान रह सकता है?
अचानक अनूप को एहसास हुआ। परमेश्वर की चुप्पी उदासीनता नहीं है। वह तो धैर्य है। वह समय दे रहा है—पश्चाताप का, सुधार का। पर जो इस धैर्य को कमजोरी समझ बैठते हैं, वे अपने लिए ही कठोर न्याय का भंडार बटोर रहे हैं। चंद्रभान का अहंकार, उसकी क्रूरता—क्या यह उसकी अपनी ही आत्मा को जड़ से काटने वाला कुल्हाड़ा नहीं है? परमेश्वर का प्रेम उसके न्याय से अलग नहीं। वह प्रेम ही है जो बुराई को अनंत तक फलने-फूलने नहीं दे सकता। उसे एक दिन काटना ही होगा, ताकि अच्छाई का पौधा साँस ले सके।
साँझ और गहरा गई। पहला तारा टिमटिमाया। अनूप का हृदय अब भारी नहीं था। वहीं चटाई पर उसने अपना माथा जमीन से लगा दिया। उसकी प्रार्थना अब शिकायत नहीं थी, न ही जल्दबाजी में माँगा गया कोई समाधान। वह एक समर्पण था। “हे मेरे चट्टान, हे मेरी शरण। तू ही मेरा सहारा है। तू ही मेरे दुख में सांत्वना देगा। मेरे पैरों को फिसलने से बचाएगा। तेरा प्रेम मुझे थामे रखेगा। और जब तू दुष्टों को उनके अपने ही बनाए जाल में फँसाएगा, तब मेरा मन यह जानकर शांत होगा कि यहोवा हमारा परमेश्वर न्यायी है।”
उस रात, अनूप की नींद गहरी थी। बाहर, आकाश में बादल फिर से जमा हो रहे थे। दूर, चंद्रभान के महलनुमा घर में, मदिरा के नशे में धुत वह और उसके साथी जोर-जोर से हँस रहे थे। उनकी हँसी रात की खामोशी में कर्कश लग रही थी। अनूप का खेत अभी भी बाड़ से घिरा हुआ था। पर अब उसे एक अदृश्य सत्य का बोध हो गया था—न्याय की धारा बह चुकी थी। वह धीमी थी, पर रुकने वाली नहीं। और उसकी धार को मोड़ने की शक्ति किसी चंद्रभान के पास नहीं थी।